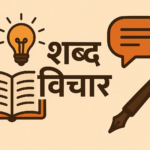धूमिल की अकाल दर्शन कविता का भावार्थ/ मूल संवेदना
धूमिल हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कवि हैं। इनका वास्तविक नाम सुदामा पांडे है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में और मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी।
अकाल दर्शन कविता उनके प्रथम काव्य संकलन “संसद से सड़क तक” में संग्रहित है जो 1972 में प्रकाशित हुआ था। “कल सुनना मुझे” काव्य संकलन के लिए इन्हें मृत्योपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ब्रेन ट्यूमर के कारण इनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो जाने से हिंदी साहित्य को अपूरणीय क्षति हुई।
धूमिल साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवियों में से हैं। व्यवस्था से असंतोष, विद्रोह, अनास्था और नैराश्य के स्वर सहित साठोत्तरी कविता की सभी विशेषताएं धूमिल के काव्य में देखी जा सकती हैं।
“अकाल दर्शन” कविता भी उनकी अन्य कविताओं की तरह व्यवस्था की कमियों पर प्रश्न उठाती एक बेहद ज़रूरी और प्रासंगिक कविता है।
उनकी कविताओं पर भदेसपन और अश्लीलता के आरोप भी लगते रहे हैं। व्यथित और आक्रोशित युवा कवि के रूप में यह भाषा उनकी प्रतिक्रिया की तरह ली जा सकती है।
भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भुखमरी की समस्या ! धूमिल ने इस कविता में इसी समस्या की पड़ताल की है और इसके कारणों की तह तक जाने का प्रयास किया है।
कविता की शुरुआत ही असली प्रश्न से होती है। कवि जानना चाहते हैं कि भूख कौन उपजाता है अर्थात किसके कारण इस भूख नाम की समस्या से सामना करना पड़ता है?
क्या भूख उस नीयत के कारण पैदा होती है जो मासूम इंसानों को घृणा की खुराक देकर उन्हें खुले में छोड़ देती हैं ? कवि द्वारा यह सवाल चालाक आदमी से किया गया। यहां यह चालाक आदमी व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा या व्यवस्था का संचालक है। उस आदमी ने (असल में सबसे ताकतवर नेता) झुग्गियों की ओर इशारा कर इधर-उधर भटकते छोटे बच्चों को इस भुखमरी का कारण बताया अर्थात उसकी नज़र में जनसंख्या की अधिकता इस भुखमरी का कारण है और ऐसा इशारा करके वह बेशर्मी से हंसने लगा।
कवि ने उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए उसे लगभग जाते हुए से रोक कर बताया कि बच्चे उस स्थिति में पैदा होते हैं जहां इंसान के पास न काम होता है न शिक्षा! ज़्यादा शिक्षित और कामकाजी लोगों के बच्चे अमूमन कम होते हैं।
लेखक कहते हैं कि यह बात इतनी तार्किक है कि इस बात से वह नीति नियंता भी सहमत हैं, जो ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे के नागरिक मानते हुए इन्हें राशन देते हैं। राजनेता तो यहां तक कहते हैं कि बच्चे ही दुनिया को रंगीन और जीने लायक बनाते हैं।
लेखक इस बात में छुपी मक्कारी को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि इस तरह अभावों और मुफ़लिसी के बीच झुग्गियों में जन्म लेते बच्चे दरअसल पेड़ों के खुशनुमा निशान नहीं बल्कि अभावग्रस्त जोड़ों का अपराध बनकर रह जाते हैं।
लेखक की समझ से घबराया हुआ आदमी जल्दी से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और जाते हुए उसकी बहुत हंसी छूट जाती है। भूख से जुड़े सवाल को सुनकर अब उसे भागने की जल्दी है क्योंकि उसे जनता के हित में बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। यहां “जनता के हित में” शब्दों के प्रयोग का गहरा व्यंग्य लिए हुए हैं।
अब लेखक स्वयं अपने किए प्रश्न से रूबरू है। भूख जैसे जानलेवा सवाल का कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता। उन्हें भूख से लड़ रहे इंसान से सामना करते नहीं बन रहा। वे वहां खाली हाथ जाने में झिझकते हैं। खाली हाथ जाना महज़ लफ़्फ़ाजी करने जैसा जो है! लेखक को डर है कि नज़दीक जाने से उन्हें मौत की ओर बढ़ते इंसान की पीठ ही दिखेगी।
और अचानक जैसे दिमाग में कोई बत्ती जली ! अपने सवाल से जूझते लेखक को जवाब समझ में आने लगा है। आज़ादी और गांधी के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाना उन्हें समझ आया।
लेखक ने आपातकाल, पाकिस्तान के साथ युद्ध और तत्कालीन परिस्थितियों देखी थी तो उन्हें इन झुनझुनों का मतलब समझ में आ रहा था।
एक तरफ तो लोग भूख से बिलबिला कर अखाद्य और निम्न गुणवत्ता का खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ मर रहे हैं। बदहाली के बावजूद भी कुछ न कुछ दान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आस्था के नाम पर आम आदमी मरता-मरता भी कुछ न कुछ देने की इच्छा रखता है।
किसी भी तरह की सभा-सम्मेलन, जुलूस में देश के नाम पर पहुंच जाना और अपनी असली समस्या को प्राकृतिक (नियति) समझकर सहजता से उसे स्वीकार कर लेना यह आम आदमी की ख़ासियत या कमज़ोरी है। इनके उदास चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं कि कल क्या होगा? दूसरे वक़्त का राशन बेशक न हो लेकिन मोहल्ले में रात्रि जागरण की संतुष्टि इनकी नीम बेहोशी दिखाती है।
लेखक ने एक प्रबुद्ध नागरिक की हैसियत से जब भी उन्हें चेताने की कोशिश की कि देश का शासन और राशन… आगे की बात कहने से पहले ही लोग उन्हें टोक देते हैं।
लेखक को अफ़सोस है कि लोग उन्हें समस्या की असली जड़ पर हाथ रखने के पहले ही रोक देते हैं। ये वे लोग हैं जिनका आधा शरीर भेड़िए (अव्यवस्था जनित स्थितियों) ने खा लिया है फिर भी वे देश (जो कि जंगल बन चुका है) की तारीफ़ करते नहीं थकते।
अपनी स्थितियों से मुतमईन ये निश्चिंत लोग कहेंगे कि भारत वर्ष नदियों का देश है। नदियां जो हर वर्ष बाढ़ के साथ उनकी तबाही भी लाती हैं, वे उनके लिए गर्व का विषय बनी रहती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से इनका कोई वास्ता नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं।
ये भोले लोग यह नहीं समझते कि उन्हें राशन के रूप में जो चारा मिलता है, वह उन्हें सिर्फ़ पालतू बना कर रखने की कवायद है। अनाज उन्हें बख़्शीश की तरह देकर वे उनसे उनकी समझ, वोट और टैक्स के रूप में ले लेते हैं।
“कभी गाय तो कभी हाय” अर्थात कभी धर्म के नाम पर तो कभी युद्ध के डर के नाम पर शीर्ष पर बैठे ये चंद लोग सभी को एक दिशा में हांकते रहते हैं।
यह सारा उपक्रम ये बड़े लोग करते कैसे हैं- लेखक इन्हें पूरी तफ़सील से समझाने का प्रयास करते हैं। लेखक इस गुत्थी को सुलझाने के क्रम में एक बेहद ज़रूरी बात कह जाते हैं कि वह कौन सा लोकतांत्रिक उपाय है कि जिस उम्र में उनकी मां का चेहरा झुर्रियों से भर गया है उसी उम्र में उनके पड़ोस की महिला के चेहरे पर उनकी प्रेमिका के चेहरे जैसी चमक है ? गरीबी और अमीरी के बीच फ़र्क को समझाने के लिए काम में ली गई ये पंक्तियां एक कटु यथार्थ है।
लोग चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। लोग जाने कैसे हो गए हैं ? लगातार के अभावों और प्रायोजित सपनों ने उन्हें जैसे अनमना कर दिया है!
लेखक की बातें सुनकर उनकी आंखों में विरक्ति, पछतावा या संकोच, कौन-सा भाव दिखता है-यह लेखक पकड़ नहीं पाते। लगभग भावशून्य हो चुके वे लोग ख़ुद परिस्थितियों से इतने पस्त हैं कि तटस्थ हो गए हैं।
लेखक सोचने लगे हैं कि इस देश में एकता युद्ध के समय याद आती है और दया अकाल के समय! क्रांति दरअसल इस देश के लिए है ही नहीं।
क्रांति के लिए जो मानसिक परिपक्वता चाहिए वह इस देश के नागरिकों में न देखकर लेकिन हमेशा क्रांति-क्रांति सुनकर वे उस क्रांति की तुलना बच्चों के शिश्न से करते हैं। जैसे बच्चे को अपने इस संवेदनशील अंग के बारे में पता नहीं होता और वह इससे खेलता रहता है, वैसे ही क्रांति के लिए जो जज़्बा, ज़िम्मेदारी और प्रतिबद्धता चाहिए वह सिरे से नदारद होने के बाद भी लोग क्रांति का आह्वान करते हैं।
कवि धूमिल की यह कविता उस फ्रस्ट्रेशन को पूरी तरह से उजागर करती है, जो सरकारों की मक्कारी और जनता की लाचारी को देख कर पैदा हुई है।
युवा गाय के नाम पर लिंचिंग जैसे अपराध करने से हत्यारे बनकर जिस तरह अपना भविष्य तबाह कर रहे हैं और मंदिर के बनने में अपने जीवन की सार्थकता महसूस कर रहे हैं, वह कवि के लिए बेचैन करने वाली बात है। महात्मा गांधी की अहिंसा और सादगी की मिसाल दे कर नेताओं की ऐश भरी ज़िंदगी उन्हें समझ में आती है। पाकिस्तान के साथ युद्ध ही नहीं मैच के समय लोगों के खून में देशभक्ति का उबाल आता है, बाकी देश के संसाधनों का दोहन, पर्यावरण का प्रदूषण, भ्रष्टाचार, अपने ही देशवासियों पर अत्याचार सब चलता रहता है – इन सब परिस्थितियों पर लेखक ने करारा व्यंग्य किया है।
कविता अपने कथ्य को स्पष्ट करने में पूरी तरह सफल है। कदाचित आज धूमिल होते तो इस कविता के शब्दों में सत्ता पक्ष को और “कड़वाहट/ नकारात्मकता” दिखाई पड़ सकती थी क्योंकि वो सबकुछ लिखने से कहां चूकते!
@ डॉ संजू सदानीरा
https://youtu.be/FXQwdJ5YfLE?si=Fk6wE8MrDGxzg6Ar