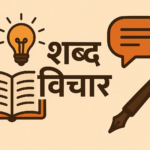पांचवा बेटा कहानी का सारांश अथवा उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
पांचवा बेटा कहानी हिंदी की मशहूर कथाकार नासिरा शर्मा की सुप्रसिद्ध कहानी है। नासिर जी हिंदी की विशिष्ट कथाकारों में गिनी जाती हैं । उनकी कहानियों में मानव मन की सामूहिक पीड़ा और सांप्रदायिकता के विरुद्ध तीखा स्वर देखा जा सकता है । उनकी हर कहानी इंसानी मां को थोड़ा और उर्वर एवं मानवीय बनती है। उनके लेखन का दायरा अन्य लेखकों से अधिक विस्तारित और मानवीय है। ताजमहल, बुतखाना और सुनहरी उंगलियां इत्यादि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। शाल्मली, ठीकरे की मंगनी, जिन्दा मुहावरे, अक्षयवट और कुइयाँजान उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं।
पांचवा बेटा कहानी में भी उनकी यही मानवीय दृष्टि प्रभावित करती है। यह कहानी भी हिंदू-मुस्लिम एकता पर लिखी गई है। आदमी-आदमी को जात-पात और मजहब के नाम पर बांटना इंसानियत के खिलाफ है । नासिरा जी ने कहानी में सहजता से दिखाया है कि कई बार व्यक्ति खुद न चाह कर भी अनजाने में ऐसा भेदभाव कर बैठता है क्योंकि उसे सदियों से यही घुट्टी में पिलाया जाता है ।
इंसानों ने दस्तूर बनाया कि मंदिर में भगवान और मस्जिद में ख़ुदा रहता है। मंदिर में मुसलमान और मस्जिद में हिंदू का प्रवेश वर्जित करके हमने आदमी आदमी के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी । इस खाई के दोनों तरफ खड़े मीठे दिलवाले लोग पाप के खौफ के कारण पिसते रहते हैं।
अमतुल एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला है। उसके चार बेटे हैं जो शहर में अच्छी नौकरी पर हैं । मोहर्रम पर अमतुल अपना इमामबाड़ा तैयार करवाना चाहती है। इमामबाड़ा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है । बारिश में कभी भी ढह सकता है अथवा छत के टपकने से इमामबाड़े में रखा सामान भीग कर नष्ट हो सकता है । वह अपनी ही कौम के रहमान से इमामबाड़े की छत की मरम्मत करवाना चाहती है लेकिन रहमान अब बेलदार (मजदूर )के बजाय ठेकेदार हो जाने के कारण उसका काम टालता रहता है।
अमतुल बहुत चिंतित रहती है और अंततः वही होता है जिसका डर था । भयंकर बारिश हो ही जाती है । इमामबाड़े में रंगीन पट, झालरें, पर्दे सजाए गए हैं, लोबान सुलगाया गया है ।
अमतुल का दिल इस बारिश से बैठा जा रहा है । मोहल्ले वालों के सामने अपनी फ़जीहत और खुदा के सामने शर्मिंदगी भी हो रही थी। बारिश का जोर थमने के बाद सुबह डरते-डरते जब वह इमामबाड़े का दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित है। लोबान की खुशबू से इमामबाड़ा महक रहा है ।
उसे पता चलता है कि यह करामात उसकी बचपन की सहेली के बेटे सुलाखी की है तो वह खुश होने के बजाय डर से सिहर जाती है। हिंदू होकर सुलाखी इमामबाड़े की छत पर गया इसका जाने क्या दुष्परिणाम हो ,यह सोचकर अमतुल की धर्मभीरू रूह कांप गई । उधर सुलाखी पूरी रात बरसती बरसात में छत को तिरपाल से ढकने में लगा रहा। पूरे ध्यान और तन्मयता से उसने इमामबाड़ा की छत को ढका। बारिश में बुरी तरह भीगने से वह सर्दी और बुखार की चपेट में आ गया। अमतुल को इसकी खबर नहीं,वह तो उससे नाराज़ थी।
मोहर्रम के दस्ते के गुजरने के बाद जब औरतें अमतुल से खाक (पवित्र भस्म) लेने आता है तो ज्योति कहारिन सुलाखी के बेटे के लिए भी ख़ाक मांगती है तब अमतुल खुद सुलाखी के न आने का जब कारण पूछती है तो उसे सुलाखी के बुखार में पड़े होने का पता चलता है। अमतुल इसे उस दिन की घटना का परिणाम मानकर डर से सिहर गई । वह उल्टे पैरों खुद ख़ाक लेकर सुलाखी के घर जाती है। उस ख़ाक को वह खुद उसके सीने पर और माथे पर मलते हुए दुआ पढती है।
सुलाखी अमतुल की बचपन की सहेली का बेटा है,जो ब्याह कर के दूर चली जाती है।शादी के थोड़े समय बाद ही एक बच्चे के बाद उसके पति की मौत हो जाती है और अमतुल उस बच्चे (सुलाखी) को बहुत प्यार करती है।
सुलाखी की बीवी भी अमतुल को सास के समान आदर देती है। सुलाखी की बीमारी के बाद अमतुल का सारा डर और गुस्सा बह गया।अब उसने इमामबाड़े की मरम्मत का सारा काम सुलाखी से करवाने की ठान ली। मोहब्बत से सर पर हाथ फेरने के बाद सुलाखी की बीवी को मजदूरी के रुपए एडवांस में देकर आसमां की तरफ दुआ में हाथ फैला कर अमतुल वहां से निकलती है। कथाकार का यह मनोवैज्ञानिक चित्रण सुलाखी के प्रति अमतुल के प्रेम को तो दर्शाता ही है, साथ ही धर्म /मज़हब के भय पर मोहब्बत की ताकत की जीत का प्रतीक बन कर भी उभरा है।
अमतुल की पोती के माध्यम से नई पीढ़ी की तर्कपूर्ण और मानवीय सोच को दर्शाना लेखिका की सकारात्मक दृष्टि का परिचायक है । अमतुल की परंपरागत सोच और उसकी पोती की आधुनिक सोच के बीच एक सीधी मुठभेड़ कहानी में रोचकता और मनोविश्लेषणात्मक मोड़ लाती है। कहानी आज की पीढ़ी की तार्किक कुशलता को दिखाने के साथ यह भी संदेश देती है कि आज का युवा आंख मूंदकर मृतप्राय परंपराओं का पालन करने में यकीन नहीं रखता। अंततः सुलाखी के घर जाकर मरम्मत का काम देना भी यही दर्शाता है।
औरतों की सामाजिक दशा तथा उन पर लादी गई पाबंदियों और उनके भीतर की जमी पीड़ा पर भी लेखिका ने संवेदनात्मक संकेत दिए हैं जहां मोहर्रम की ग़मी के बहाने औरतें अपने सीने में दबे-छुपे दर्दों पर भी आंसू बहा लेती हैं।
दूर बैठे चार बेटों के बजाय पास रहकर मुसीबत के वक्त काम आने वाला पड़ोसी बेटों से ज्यादा करीब और प्रेम का हकदार होता है। पैसों से ज्यादा इंसान को प्यार और वक्त की जरूरत होती है । लेखिका इस बात को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह सफल रही हैं।
कुल मिलाकर यह कहानी एक संदेश प्रधान कहानी है । इस कहानी के माध्यम से सदियों की दम तोड़ती परंपराओं के ऊपर नई सोच की, धार्मिक कट्टरवाद और मजहबी खाप के ऊपर इंसानी मोहब्बत की ताकत की जीत को दर्शाया गया है। आज इंसान को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है ।लेखिका बताने में पूरी तरह सफल रही है कि धार्मिक आडंबरों से ज्यादा महत्त्व इंसानी जज्बातों का है । आपसी प्रेम ,भाई चारा और सिस्टरहुड जीवन रूपी मशीन के लिए सबसे जरूरी तत्त्व है। कहानी आज के परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक है।
© डॉ. संजू सदानीरा