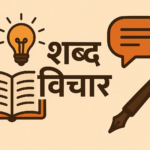मोहन राकेश के नाटकों में प्रयोग और प्रभाव/ मोहन राकेश के नाट्य लेखन की विशेषताएं
भारत में संस्कृत साहित्य में नाट्यशास्त्र और नाट्य विधा की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। उसी से प्रेरित हिंदी नाटक भी अपना एक भव्य अतीत और आशान्वित भविष्य रखता है । नाट्य विधा की इस परंपरा को नित-नवीन रूप देने में जिन प्रखर प्रतिभाशाली नाटककारों का अमूल्य योगदान रहा है, मोहन राकेश भी उनमें से एक हैं । सच तो यह है कि नाटक को “नया नाटक” और “यथार्थ नाटक” की उपमा दिलाने में उनके योगदान को रेखांकित किए बगैर नाट्येतिहास के अध्ययन में आगे बढ़ाना कठिन भी है और अन्यायपूर्ण भी !
इसी के साथ रंगमंच को विकसित करने में भी उनका अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान है। नाटक को वास्तविक अर्थों में रंगमंच से जोड़ने में उनके स्तुत्य प्रयास रहे हैं जो कि उनके व्यापक चिंतन और विश्व के अन्य अन्य नाट्य रूपों और रंगमंचों के अध्ययन का प्रतिफल रहा है।
उनकी लिखी तीन महत्त्वपूर्ण नाट्य कृतियां हैं –आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे । पहले दो नाटकों के आधार पौराणिक है पर आधे अधूरे पूर्णतया कल्पनाश्रित (सच्ची घटनाओं पर आधारित) नाटक है जिसमें दांपत्य जीवन की विसंगतियों का बेबाकी से उद्घाटन हुआ है ।उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि उनके सभी नाटक रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत सफल रहे हैं और अद्यतन मंचित किए जा रहे हैं।
आधे अधूरे ने लेखक की कल्पना शक्ति के साथ-साथ यथार्थ के कठोर धरातल के साथ उसकी (नाटक की) कदम ताल को बखूबी दिखाया है। मोहन राकेश से बहुत पूर्व तक हिंदी नाटक समकालीन जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बन पाया था। अधिकांश नाटक ऐतिहासिक तथ्यों का आधार लेकर आदर्शवादी, रोमांटिक और राष्ट्रीय भावनाओं को ही व्यक्त कर रहे थे। मोहन राकेश के नाटकों के माध्यम से आधुनिक जीवन की विकट स्थितियों तथा मानव-मन की जटिलताओं को अभिव्यक्ति मिली।
सबसे पहले उनके नाटक “आषाढ़ का एक दिन” को देखें तो कथा का आधार जरूर पौराणिक है परंतु उनके स्पष्ट तार आधुनिक जीवन से जुड़े हैं। कालिदास, मल्लिका, अंबिका, मातुल और विलोम व कुछ अन्य गौण पात्रों के माध्यम से कथा जो कुछ भी कहती है -अपने संपूर्ण अर्थों के साथ मन को मथती है। चाहे दुविधाग्रस्त कालिदास हो, चाहे एकांत प्रेयसी मल्लिका हो, मानगर्विता प्रियंगुमंजरी हो, पुत्री के दुख से घायल अंबिका हो -सभी यथार्थ जगत के मानव प्रतिरूप है। शायद यह हिंदी का पहले ऐसा यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ की समन्विति एवं अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ देखता और प्रस्तुत करता है।
कालिदास के बारे में पढ़ते हुए आदि कवि कालिदास नहीं वरन् एक स्वयं में सिमटा, सकुचा, आत्मप्रेमी कवि आभासित होता है। नाटक आदि से अंत तक अपने भाषिक सौंदर्य, संवाद सौंदर्य, परिस्थितियों और वातावरण – निर्माण से कथा को उभारने की दक्षता से युक्त रहा है ।
प्रथम अंक से ही जब मल्लिका कालिदास के साथ पर्वत शिखर पर वर्षा का आनंद उठाकर आती है तो प्रकृति का जो चित्र नाटककार ने खींचा है वह सुंदर दृश्य बिम्ब की रचना करता है। यूं भी इस नाटक के बिंब विधान की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी । अंबिका के साथ मल्लिका की, कालिदास के संबंध में होने वाली बहसें स्त्री स्वातंत्र्य, भावुकता, पीड़ा की तीखी भावना और वात्सल्य जैसे कई रूपों का दर्शन कराती है।
जगह-जगह सूक्त कथन भी प्रयुक्त हुए हैं ,जैसे- “जीवन की स्थूल आवश्यकता है ही तो सब कुछ नहीं है मां! उनके अतिरिक्त भी तो कुछ है ।” “किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है।”” योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है ।”
“वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता।” “व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं । ”एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक परंतु दरिद्र नहीं छिपता। सौ-सौ गुणों से भी नहीं छिपता। नहीं, छिपता ही नहीं सौ-सौ गुणों को छा लेता है। एक-एक कर नष्ट कर देता है।”
संवादों में जो सौंदर्य, व्यंग्य और मारक प्रभाव है उसे कालिदास-विलोम, विलोम और मल्लिका,अंबिका और मल्लिका के संवादों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है।
अपने दूसरे नाटक “लहरों के राजहंस” में नाटककार ने अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरनंदन को कथा का आधार बनाया है। डॉ सुरेश अवस्थी के अनुसार “लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है।”
चुनाव न कर पाने की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है।
लहरों के राजहंस में राजहंस कामना युक्त विलासप्रिय व्यक्ति मन का प्रतीक है। श्वेतांक, श्यामांक, अलका इत्यादि पात्रों के साथ सुंदरी और नंद के कथोपकथनों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है और अपने सारगर्भित अंत को प्राप्त करती है।
इस नाटक के संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर रचित “उर्वशी” प्रबंध काव्य की निम्न पंक्तियां प्रासंगिक हैं-
किंतु रस के पात्र को ज्यों ही लगाता हूं अधर से
घूंट या दो घूंट पीते ही अतल से नाद यह आता-
अभी तक भी न समझा!
दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है
रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है।
नंद अंत तक समझ ही नहीं पाता कि उसे काम (सांसारिक सुख) चाहिए या राम (संन्यास)! लेकिन न खुदा ही मिला न विसाले सनम!
सुंदरी (अपनी रानी) की लटों से खेलने की ख्वाहिश और जीवन से भागने की बड़ी ही दुर्दमनीय चाह के बीच का उसका अन्तर्द्वन्द्व कश्मकश में पड़े हर इंसान की अपनी व्यथा है। एक मिथकीय कथा के माध्यम से मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस में आधुनिक मानव की अनिर्णय की स्थिति का सटीक चित्रण किया है।
इसके साथ ही सुंदरी का बुद्ध के संन्यास के लिए यशोधरा को दोषी मानना इस सामान्य भावना को प्रबल करना है कि पत्नी से विमुखता का कारण स्वयं पत्नी होती है। सुंदरी को अपने रूप पर न सिर्फ अभिमान है बल्कि उस रूप की शक्ति पर अटूट विश्वास भी है। उसे लगता है कि वह अपनी रूप राशि के आकर्षण से कभी नंद को निकलने नहीं देगी। यशोधरा की सादगी को वो चुनौती और उपहास के अर्थ में लेती है।
नंद का बौद्ध धर्म से लगाव और फिर सुंदरी के लिए भटकाव एक अलग किस्म के तनाव को जन्म देता है। अंत में नंद आधा संन्यासी और आधा पति बन कर अभिशापित होता है। एक अवसादपूर्ण वातावरण में नाटक की समाप्ति होती है, जहां सबकुछ उजड़ चुका होता है।
इनका तीसरा नाटक है “आधे अधूरे”। यह उनका पूरी तरह यथार्थ पर आधारित नाटक है। नये प्रयोग और जीवन की जटिलताओं का व्यक्तिगत अनुभव इस नाटक को वह पैनापन देता है जो अपने आप में अनूठा है।
अधेड़ उम्र की स्त्री सावित्री और उसके जीवन में किसी न किसी भांति जुड़े पांच पुरुष पात्रों की अपने आसपास की कथा कहता एक मार्मिक और व्यंग्यात्मक नाटक है आधे अधूरे!
नाटक के मंचन में मोहन राकेश ने सभी पुरुष पात्रों का किरदार एक ही अभिनेता से अदा करवा कर एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। उनके अनुसार सभी के बाहरी लबादे, उनकी हैसियत और कार्य के अनुसार अलग-अलग हैं लेकिन वस्तुत: सभी भीतर से एक जैसे ही हैं।
जो महेंद्र नाथ सावित्री को इतना चुभता है,वह अच्छा लगता अगर वह महेंद्रनाथ न होकर कोई और होता । जिससे सावित्री शिकायत कर रही है, वह उसका पति होता तो कदाचित उसे महेंद्रनाथ अच्छा लगता। ये जुनेजा, सिंघानिया सब आज आकर्षक लग रहे,कल बुरे लगते! पतियों के लिए भी यही बात सही है।
इस नाटक की तासीर इतनी प्रभावशाली है कि आप इसके असर से बरसों बरस मुक्त नहीं हो सकते। घर के टोटे, किशोर उम्र की बेटी का हर प्रकार से जिज्ञासु होना, स्कूल में अपमानित होने के डर से स्कूल न जाना सब सच है।
सावित्री और महेंद्रनाथ की लड़ाई, महेंद्रनाथ का गुस्से में घर छोड़ कर दोस्त के यहां चले जाना, इनके बेटे अशोक की निरूद्देश्य भटकन, बेटी का भाग कर शादी कर लेना, छुटकी का मुंहजोर होना सब कुछ इस हद तक विश्वनीय है कि कभी-कभी तो इसके नाटक न होकर पड़ोस की सच्ची कहानी का भ्रम होने लगता है।
कथानक की कितनी ही बातें चौंकाती हैं जैसे उनकी बड़ी बेटी का उस घर से चले जाने का कारण उस घर की हवा में ही कुछ ऐसा बताना कि जिससे दम घुटता है। बेटे का सावित्री के बॉस के सामने का व्यवहार।
दाम्पत्य संबंधों की असलियत को लेखक ने जैसे उधेड़ कर रख दिया है! इसके साथ ही अभाव में जीती एक अधेड़ उम्र की महिला की जीवन जीने की ख्वाहिश भी नज़र आती है। जब सावित्री बाहर जाने से पहले आईने में अपना चेहरा देख कर सोचती है कि अभी सबकुछ पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि जिया न जा सके तब उसकी जीजिविषा को समझा जा सकता है।
मां बाप के बीच कलह से बच्चों के प्रभावित होने और गरीबी के कारण पड़ने वाले परिणामों को भी दिखाने में मोहन राकेश कामयाब रहे हैं।
कुल मिलाकर मोहन राकेश ने अपने तीनों नाटकों के माध्यम से तीन अलग-अलग कथाओं को उठा कर उन्हें जीवन के विविध रंगों से जोड़ कर बहुत खूबसूरत और प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है।
© डॉ. संजू सदानीरा
https://youtu.be/HSHNK5PwxbM?si=w25bbmvGp0naMbgf
https://youtu.be/9cJTpcg7frA?si=e19x_THsCui-AZlm