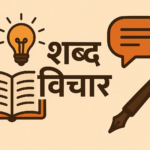विवाह: स्त्री आज़ादी का अपहरण
हमारी छोटी से छोटी चीज़ पर कोई बेजा हक़ जमाये तो हम चीख पड़ते हैं, कीमती चीज़ हो तो हम कानून की शरण लेते हैं, लेकिन हमारा पूरा भविष्य, निर्णय शक्ति ही नहीं, जीवन तक लगातार हायजैक किया जा रहा है, “उड़ाया” जा रहा है, और हम इत्मीनान से जीते चले जा रहे हैं। कोई विरोध में हल्की-सी बाँह ऊँची भी करे तो उसे नालायक ही नहीं अप्राकृतिक और असामाजिक तक ठहराये जाने की साजिश बदस्तूर जारी है।
एक लड़की “शादी नहीं करनी है”, ये कहना तो दूर,”अभी नहीं करनी” है, कह दे तो हजारों भृकुटियों में बल आ जाते हैं। जितनी लडकियों से बात होती है,उनमें से अधिकतर तो शादी ज़रूर करना चाहती हैं क्यूंकि ये तो “होनी ही है”, “होती आई है” (परंपरा है)।जो कुछेक “कुछ और” करना चाह रही, उनको पता नहीं कि वो कुछ और क्या है?
एक दिन कॉलेज से घर आई तो कोई महापुरुष (पढ़ें मक्कार पुरुष) आये हुए थे। बातचीत चल रही थी बाकी घरवालों से। बातचीत का जो हिस्सा मुझे सुना, उसमें वो फरमा रहे थे कि “न,न, हम ऐसी ग़लती ही नहीं करते” (मैं चौंकी कि कौन-सी ग़लती भई?)आगे की बातचीत में उनका कहना था कि घर के किसी लड़के के लिए लडकी “देखनी” हो तो पहले ही तय कर लेते हैं कि ज्यादा पढी-लिखी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा पढ़ी-लिखी होगी तो नौकरी करेगी, फिर हजार नखरे दिखाएगी, घर का कोई काम करना पसंद नहीं करेगी, झगड़े होंगे, गृहस्थी संभालनी मुश्किल होगी। वगैरह ,वगैरह।
यूँ तो जाने कितनी ही बार ये सब सुना था। उस दिन बंद कमरे में सुन रहे ये शब्द पिघला शीशा लगे।
मतलब सदियों से हमारी जाने कितनी पीढियां ख़त्म हो गई यूँ कंट्रोल होते-होते,गुलाम बनते!!!कौन कहता है कि दास प्रथा खत्म हो गई। गुलामी के युग बीत गये! विवाह इन सबका परिष्कृत (?) और लुभावना रूप है और कुछ नहीं। खाना पकाना, बरतन धोना, बच्चे पालना, घर संभालना, बिना पूछे कहीं आना-जाना नहीं- सब वही तो है। बस यहाँ आपका नामकरण गृहमंत्री/गृहलक्ष्मी हो गया, वो भी बहुत जगह तो लल्लोचप्पो माना जाता। आप अपने मालिक के घर में उसके साथ रह सकती हैं। (इसकी अलग ही कीमतें होती हैं)। सबसे बड़ी बात ये कि जो लेख की शुरुआत में कहा कि अहसास तक नहीं किसी को इन बातों का। इससे उल्टा यानी यही शर्तें शादी के पहले लड़के के लिए लगाया जाना अकल्पनीय है कि लड़का नौकरी-वौकरी न करे, लड़की अच्छा कमाती है, ये तो घर संभाले। आराम से घर में रहकर घर का काम करे, पैसे की कोई कमी लड़की होने नहीं देगी। तो, सच मानिए, भारत में शादियां होनी बंद हो जाएंगी।
हद तो यह है कि लड़कियां इस विस्थापन और घरों में बंद रहने के लिए इस हद तक कंडिशंड हैं कि अपना भला सुनकर भी चौंक जाती हैं। न सिर्फ़ चौंक जाती हैं बल्कि (कु)तर्क देती हैं। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट और बाद में कलीग युवा लड़की ने कहा था -“मैम ये जब से औरत बाहर कमाने जाने लगी है, घर तभी से फूटने लगे हैं, और कमाने भी इसलिए जाती हैं कि खुद के खर्चे बढ़ा लिये, वर्ना काम चलता ही था,कौन-सा लोग भूखे सोते थे।” कह तो बहुत कुछ सकती थी, नहीं कहा कि कहाँ से, क्या शुरुआत करूँ। कैसे कहूं कि कितने घरों की औरतों पर उसने यह सर्वे किया है, जहां औरतों की कमाई उनके अपने ऊपर खर्च होती है? हालांकि बाद में इस पर उससे बहस और चर्चा हुई थी कि कैसे विवाह के बहाने औरतों के श्रम पर पूरी पितृसत्ता टिकी है।
परिवार का वर्तमान ढांचा पूरी तरह महिलाओं के मुफ्त श्रम पर खड़ा है। जिस दिन लड़कियों को इस साज़िश का आभास होने लगेगा, विवाह से उनका मोहभंग होने की शुरुआत हो जाएगी। कामकाजी महिलाओं के नाम पर जिस तरह औरतों का विभाजन और शोषण हो रहा है,वो अलग से चर्चा की मांग करता है। हकीकत में कोई भी लड़की/औरत ऐसी नहीं है,जो कामकाजी न हो, हां सैलरी बहुत कम को मिलती है। महान कम्युनिस्ट रोज़ा लग्ज़मबर्ग की न भूलने लायक युक्ति याद आ गई – “जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मागेंगी, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी।”
गृहिणी के गर्व के नाम पर जिम्मेदारियों और उलाहनों के अतिरिक्त उनके पास उल्लेखनीय कुछ भी नहीं। न कोई प्रॉपर्टी उनके नाम होती है। कहीं जाने, कुछ भी पहनने की “इजाजत” पति और ससुराल वाले आसानी से दे देते हैं, वे इसी में मुग्ध होने को प्रशिक्षित हैं। जबकि सच यह है कि उनकी इच्छा के अनुसार खाने पहनने को लड़कियां अपनी आदतों में ढाल लेती हैं। यहां तक कि स्लीवलेस ब्लाउज़, छोटे बाल और ऐसी ही मामूली ख्वाहिशें वो आगे के लिए टाले रखती हैं।
लिंग आधारित प्रशिक्षण, भेद-भाव युक्त परवरिश और बचपन से स्ट्रॉन्ग रोल डिवीजन ने बदलाव को बहुत धीमा कर रखा है। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक अगर लैंगिक समानता पर काम इसी धीमी गति से चला तो कम से कम डेढ़ सौ साल लगेंगे समानता आने में। तब तक शादी की शॉपिंग होती रहेगी, दहेज का सामान जुटता रहेगा, लड़की गाजे बाजे से विदा होती रहेंगी और जो इससे वंचित रह जाएंगी,वो कुढ़ती रहेंगी (ससुराल की प्रतीक्षा में व्यग्र बहुत सी युवतियां देख ली हैं,जो निराशाजनक है)। जिन लड़कियों की शादी सामाजिक रूप से स्वीकृत तय उम्र तक नहीं होती, उन्हें जीवन से बेज़ार देखना, उनके माता-पिता को दयनीय देखना स्वस्थ समाज का द्योतक नहीं है।
दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भोर तो क्या भोर की आहट भी नहीं है। मटमैला-सा उजास जो कहीं-कहीं किसी परिवार में दिख रहा है,उसी को देखकर तसल्ली तो न हो रही।
वो सुबह कभी तो आयेगी।
© डॉ. संजू सदानीरा