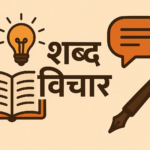शिक्षा के सही मायने/ शिक्षा का उद्देश्य या असली शिक्षा
शिक्षा जैसी व्यापक अवधारणा पर अपने लेख का प्रारंभ मैं अंग्रेजी की पंक्ति से करना चाहूंगी- ”Education is the third eye.” अर्थात जो कुछ भी हमें अपनी दो पार्थिव आंखों से दिखाई नहीं देता वह हमें शिक्षा रूपी आंतरिक आंखों से दिख जाता है। पॉकेट में पैसे और आंखों पर चश्मा होने के बावजूद सफर पर निकले व्यक्ति के लिए शहर का नाम पढ़ना उतना ही नामुमकिन है जितना बिना ज़ुबान के बोलना। यानी शिक्षा वास्तव में तीसरी लेकिन सबसे सक्षम आंख है जिससे बिना आंख वाले भी दुनिया देख और समझ सकते हैं।
सवाल है कि क्या शिक्षा आज तीसरी आंख का कार्य कर रही है? शिक्षा जैसे बहु आयामी शब्द का प्रयोग आज अत्यंत संकीर्ण अर्थ में हो रहा है हमने देखा कि दो पार्थिव आंखों से जो हम नहीं देख पाते उसे देखने में जो समर्थ बनाए वह सच्ची शिक्षा है। खाली दिमाग को खुले दिमाग में जो बदले, वह शिक्षा है। साक्षरता अक्षर ज्ञान करा सकती है लेकिन शिक्षा सही अर्थों में न दी जाए तो व्यक्ति का भावनात्मक विकास नहीं हो पाता। भावनात्मक विकास से विद्यार्थी एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार होता है, जो देश के लिए ज़रूरी है।
परंतु दुनिया भर के शिक्षालय मिलकर भी क्या यह पुनीत कार्य कर रहे हैं? आज जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है,उसमें सफलता अंतिम सीढ़ी है और इस सफलता के भी सीमित मायने हैं। साल भर कक्षा में किताबी ज्ञान की भरपूर खुराक शिक्षार्थी को दी जाती है और अंततः परीक्षा भवन में अपनी उत्तर पुस्तिका में वह अपनी संपूर्ण खुराक की उल्टी कर देता है। भारी भरकम शब्दों में रहते-रटाएं उत्तर के आशिक अर्थ से भी बच्चे का सरोकार नहीं होता है।
एक और सूत्र वाक्य है जिसका प्रयोग विशेष शिक्षण संस्थान करते रहे हैं -”सा विद्या या विमुक्तये।” अर्थात विद्या वह है जो बंधन मुक्त करती है। क्या वास्तव में आज विद्या मुक्त कर रही है? मुक्त करने के नाम पर उन्हें और बांधा जा रहा है। हिंदू विद्यालय अपने विद्यार्थियों को कट्टर हिंदू बना रहे हैं,मदरसे सच्चा मुसलमान बना रहे हैं। क्या कोई भी शिक्षण संस्थान सच्चा इंसान बनाना तो दूर, बनाने की बात भी करता है?
राष्ट्रीयता के नाम पर अहं, जातीयता के नाम पर अहं ! “वसुधैव कुटुंबकम्” वाले देश में आपस में ही कुटुंबट रहना दूभर है। यह कैसी शिक्षा है? परंपराओं के नाम पर अतीत का अंधानुकरण और धर्म के नाम पर अनौचित्यपूर्ण व्यवहार -यह हमारी शिक्षा पद्धति नहीं होनी चाहिए। यहां ओशो की बात याद आ रही है- “क्या यह उचित नहीं है कि अतीत का भार हमारे सिर पर न हो? वह है पैरों के तले की भूमि बने, यह तो ठीक लेकिन सर का बोझ बने, यह तो ठीक नहीं है।”
हर जगह शिक्षा के नाम पर अनुशासित व्यक्तित्व के निर्माण का दंभ पाला जा रहा है जबकि उचित तो यह है कि शिक्षा आत्मविवेक दे,अनुशासन नहीं। जो जितना अनुशासित है, वह उतना निर्जीव है । अनुशासन के बजाय स्वविवेक अर्थात आंतरिक शासन लगता है आज की शिक्षा पद्धति के बूते के बाहर के बात है। या तो दमन होगा या उच्श्रृंखलता! तीसरी बात ही नहीं!
पचास-पचास, सौ-सौ बच्चों को एक कक्षा में एक तरह से डंडे से हांका जा रहा है जबकि उन पचासों का दिमाग अलग-अलग क्षमता वाला है। फैक्ट्री के माल की तरह बस उत्पाद तैयार हो रहे हैं। वे अपना दिमाग न लगाना चाहते हैं, न लगाना जानते हैं। जो बच्चे अपना दिमाग लगाना चाहते हैं उन्हें भी भेड़चाल का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जाता है।
महान विचारक गेटे की एक प्रसिद्ध उक्ति जीवन का मूल मंत्र होनी चाहिए-” ज्ञान शंकाओं को जन्म देता है।” पर जो पढ़ाया जा रहा है वह शंकाएं नहीं है महज समाधान है और जहां शिक्षा समाधान से प्रारंभ होती है- मुक्ति का, उन्नति का मार्ग बंद हो जाता है। पहले प्रश्न हो फिर उसका उत्तर ढूंढा जाए, यह नहीं कि उत्तर पहले से तैयार है और तैयार उत्तर के अनुसार प्रश्न बनाए जाएं। ये प्रश्न भी बने बनाए ही होते हैं।
यह प्रत्यक्ष है कि जो प्रश्नाकुल हैं,जिज्ञासु हैं- वही संसार को नया ज्ञान देते हैं। शिक्षा की शुरुआत अतीत के उदाहरणों, आदर्श व्यक्तियों और समाधानों से होने के कारण हमें बार-बार मुड़कर कोई समस्या आने पर पीछे देखना पड़ता है परंतु समाधान चूंकि पुराने और प्रश्न नए हैं इसलिए हम ठोकर खाते हैं।
एक गहन सुरंग में एक दूसरे को धक्का देकर दीवार को छू-छू कर टटोलकर हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास नए उदाहरण, नए आदर्शों और नई समस्याओं के लिए नये समाधानों को देख सकते की दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है क्योंकि विकसित होने नहीं दी गई। बचपन से सिखा- बता दिया गया कि हमारे आदर्श क्या है, परंपराएं क्या है और किन से आगे जाकर नहीं सोचना है।
सच तो यह है कि एक शिक्षक को क्रांत द्रष्टा और विद्रोही होना चाहिए। शिक्षक अपने विद्यार्थियों में प्रश्न करने की सामर्थ्य पैदा करें , उन्हें अपनी नयी सोच विकसित करने को प्रेरित करे पर इसके विपरीत आंतरिक सवालों को दबाकर बाह्य प्रश्नों के बाह्य उत्तर दे दिए जाते हैं। शिक्षक खुद इस पूंजावादी व्यवस्था में एक नये प्रकार का मजदूर है, जिसके हाथ में नीति निर्धारण है ही नहीं। व्यवस्थाजनित कुंठा भी उसे ज्यादा सरोकार रखने से रोकती है और व्यक्तिगत/ मानसिक स्थिति भी।
जो विद्यार्थी सचमुच विद्यार्थी (विद्या +अर्थी) अर्थात विद्या के लिए इच्छुक हैं,वे बहुधा इस व्यवस्था से कुंठित हो जाते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर पुस्तकीय ज्ञान से जुड़े हैं,उतने से ही सरोकार रखने वाला शिक्षक दोबारा पूछने पर दंड की भाषा में बात करता है जबकि शिक्षक के हाथ में छड़ी उसकी सबसे बड़ी असफलता है।
कोई शिक्षक जब तक अपने विद्यार्थियों से एक सुदृढ़,स्नेहिल संबंध नहीं जोड़ सकता, तब तक वह अपने अंदर का ज्ञान उनमें पल्लवित कर सकता है- इसमें संदेह है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध मार्केट बेस हो गया है। विद्यार्थी ग्राहक हो गए हैं और शिक्षक सर्विस प्रोवाइडर! जब से यह व्यवस्था बनी है तब से स्थिति विकट से विकटतर हो रही है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का सौहार्दपूर्ण और आत्मीय संबंध सीखने- सिखाने की प्रक्रिया को अत्यंत रोचक और भावमय बना सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि एक बड़े पैमाने पर हम इस तथ्य को भूलते जा रहे हैं।
आज की शिक्षा व्यवस्था के प्रश्नों और समाधानों को वैश्विक होना पड़ेगा। संकुचित राष्ट्रीयता की अवधारणा से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व समुदाय (आखिरकार सभी देश एक ही धरा पर स्थित हैं) के हित के प्रति सचेत होना होगा। देशों के बीच की आपसी कटूता और दुश्मनी सही शिक्षा के माध्यम से ख़त्म की जा सकती है। अमन -चैन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है और राष्ट्रीयता की खुराक़ के माध्यम से युद्धों को संभावित बताना शिक्षा के माध्यम से सरल कर दिया गया है।
नदियां, पहाड़, जंगल से हमें प्रेम करने वाली शिक्षा बाल मन में प्रारंभ से डालनी होगी। महिला विरोधी मानसिकता और जातिवादी प्रैक्टिसेज के ख़िलाफ़ मानस तैयार करना शिक्षा की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। विचार और तर्क से प्रेम, कुरीतियों का विरोध,मानवता की विरोधी ताकतों से घृणा और इंसान ही नहीं जीव मात्र से प्रेम की शिक्षा देनी होगी। अन्यथा हम आज जो दे रहे हैं वह शिक्षा जिस थाली में खाए उसी में छेद करना सिखा रही है। सौहार्द, एम्पैथी और सामंजस्य नहीं!
ऐसी गला काट प्रतिस्पर्धा और रटंत विद्या का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिक्षा पद्धति में बदलाव अत्यंत अपेक्षित है। इसके साथ ही साइंटिफिक टैम्पैरामेंट को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति के साथ-साथ व्यवहारिक शिक्षा, कला और मानसिक उत्थान के अभ्यास को किसी न किसी तरह से पाठ्यक्रम से मजबूती से जोड़ना बहुत जरूरी है।
© डॉ. संजू सदानीरा
https://youtu.be/OY1NXdlbLJ4?si=LFhyCFM_Pe1etHr_